
ब्लैकआउट के नियम
पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई जिसके बाद पूरे देश में आतंक के खात्मे के लिए उबाल देखा जा रहा है। इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव के बीच भारत में सात मई को युद्ध की संभावना को देखते हुए नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल किया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को मॉक ड्रिल को लेकर दिए गए निर्देशों में, 54 वर्षों में पहला “क्रैश ब्लैकआउट उपायों के प्रावधान” को भी बताया गया है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये ब्लैकआउट क्या होता है? तो बता दें कि युद्ध के दौरान दुश्मन के विमानों द्वारा हवाई हमलों के दौरान ब्लैकआउट लागू किया जाता है। ब्लैकआउट का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के हवाई हमलों को मुश्किल बनाना है ।
ब्लैकआउट की आवश्यकता क्यों है
ब्लैकआउट लगाने की आवश्यकता क्यों है तो इसका जवाब है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामान्य दृश्यता स्थितियों के तहत ज़मीन से 5,000 फ़ीट की ऊंचाई पर कोई भी रौशनी दिखाई ना दे ताकि दुश्मन के विमान को हमले के लिए नागरिक क्षेत्र दिखाई ना दे। ब्लैकआउट का उद्देश्य “लोगों को रात में दुश्मन के विमानों से खुद को और अपने शहरों को सुरक्षित रखने में सक्षम बनाना है, बिना पूर्ण अंधेरे की असुविधा के।”

भारत पाकिस्तान युद्ध के हालात
ब्लैकआउट के दौरान क्या करें, क्या नहीं
किसी भी इमारत में कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो उसे अपारदर्शी सामग्री से ढक देना चाहिए।
किसी चमकदार लाइट इमारत के छत वाले हिस्से के बाहर दिखाई नहीं देनी चाहिए।
इमारत या उसके किसी भी हिस्से के बाहर ऊपर की ओर कोई चमक नहीं होनी चाहिए।
किसी भी इमारत के बाहर सजावट या विज्ञापन के लिए कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए।
ब्लैकआउट के दौरान कार में लगने वाली सभी लाइट्स को स्क्रीन किया जाना चाहिए, जिनसे बीम निकलती हैं।
इसके लिए पहला तरीका है कांच के ऊपर सूखा भूरा कागज़ लगाना, जिससे हल्की रोशनी निकलेगी।
दूसरी विधि कांच के पीछे एक कार्डबोर्ड डिस्क डालना है जो पूरे क्षेत्र को कवर करती है।
रिफ्लेक्टर को इस तरह से कवर किया जाना चाहिए कि रिफ्लेक्टर से कोई लाइट ना निकलती हो।
हाथ में किसी तरह की रौशनी हो तो उन्हें भी कागज़ में लपेटा जाना चाहिए।

ब्लैकआउट के बारे में जानें
कैसे जारी की जाती है हवाई हमले की चेतावनी
दुश्मन के विमानों के आने की चेतावनी जारी करने का काम वायु सेना करती है। जैसे ही वायु सेना को दुश्मन के आने वाले विमान का पता चलता है, इसकी सूचना क्षेत्रीय नागरिक सुरक्षा नियंत्रण केंद्रों को भेज दी जाती है, जो इसे शहर के केंद्रों को भेज देते हैं जो ज़मीनी कार्रवाई शुरू करते हैं। जहां तक वायु सेना का सवाल है, यह सूचना को एक बड़े नक्शे पर अंकित करती है और रक्षात्मक जवाबी कार्रवाई की योजना बनाती है। हवाई हमले की चेतावनी आम नागरिकों को बचने का मौका देती है।

हवाई हमले की चेतावनी
कितने तरह की होती है हवाई हमले की चेतावनी
हवाई हमले की चेतावनी के संदेश चार प्रकार के होते हैं-
‘हवाई हमले का येलो अलर्ट’ यह एक प्रारंभिक और गोपनीय संदेश होता है और यह दुश्मन के विमान की गतिविधि का पूर्वानुमान होता है। इस संदेश के मिलते ही नागरिक सुरक्षा को बिना किसी बाधा के आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। सार्वजनिक अलार्म को कम करने के लिए इस चेतावनी को गोपनीय रखा जाता है।
‘हवाई हमले का रेड अलर्ट’ यह एक चेतावनी होती है कि दुश्मन के विमान कुछ शहरों की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ ही मिनटों में उन पर हमला हो सकता है। यह संदेश नागरिक सुरक्षा प्रतिक्रिया के उन हिस्सों को मिलता है और यह कार्रवाई के लिए आह्वान होता है। इस अलर्ट के बाद सायरन के माध्यम से सार्वजनिक चेतावनी दी जा सकती है।
‘हवाई हमले का ग्रीन अलर्ट’ इसका मतलब है कि हमलावर विमान शहरों को छोड़ चुके हैं या अब उन्हें कोई खतरा नहीं दिख रहा है।
‘हवाई हमले का व्हाइट अलर्ट’ यह तब भेजा जाता है जब ‘हवाई हमले का संदेश-पीला’ में चेतावनी दी गई प्रारंभिक धमकी गुज़र जाती है। इस प्रकार का अलर्ट भी गोपनीय होता है।
20वीं सदी में ब्लैकआउट की प्रथा प्रचलित थी
ब्रिटेन में ब्लैकआउट की शुरुआत:1 सितंबर 1939 को युद्ध की घोषणा से पहले हुई थी
अमेरिका में ब्लैकआउट की शुरुआत पर्ल हार्बर हमले (7 दिसंबर, 1941) के बाद पश्चिमी और पूर्वी तटों पर की गई थी।
युद्ध के पहले ब्लैकआउट की प्रथा मुख्य रूप से 20वीं सदी में द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) के दौरान प्रचलित काफी प्रचलित थी।
भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच पंजाब के फिरोजपुर में ब्लैकआउट का अभ्यास शुरूकिया गया है। हालांकि, आधुनिक युद्ध में सैटेलाइट और रडार तकनीक के कारण ब्लैकआउट की प्रभावशीलता कम हो सकती है, फिर भी यह रणनीति आपातकालीन तैयारियों और नागरिक सुरक्षा का हिस्सा बनी हुई है।

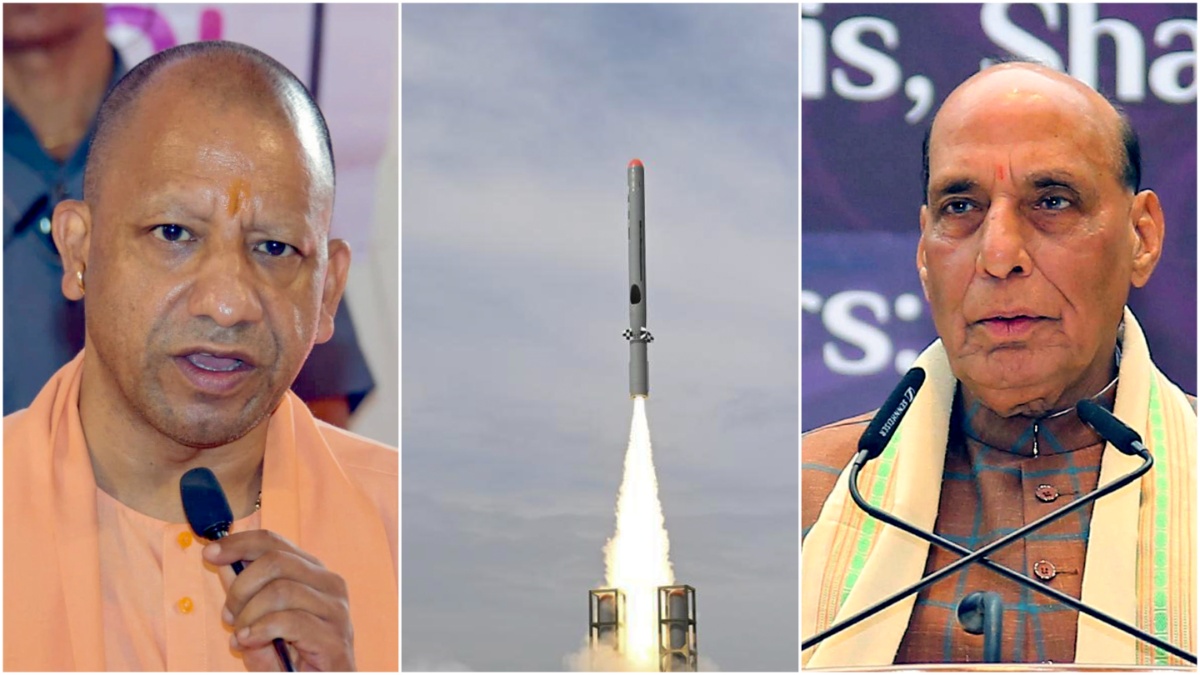










 Users Today : 19
Users Today : 19 Views This Month : 424
Views This Month : 424